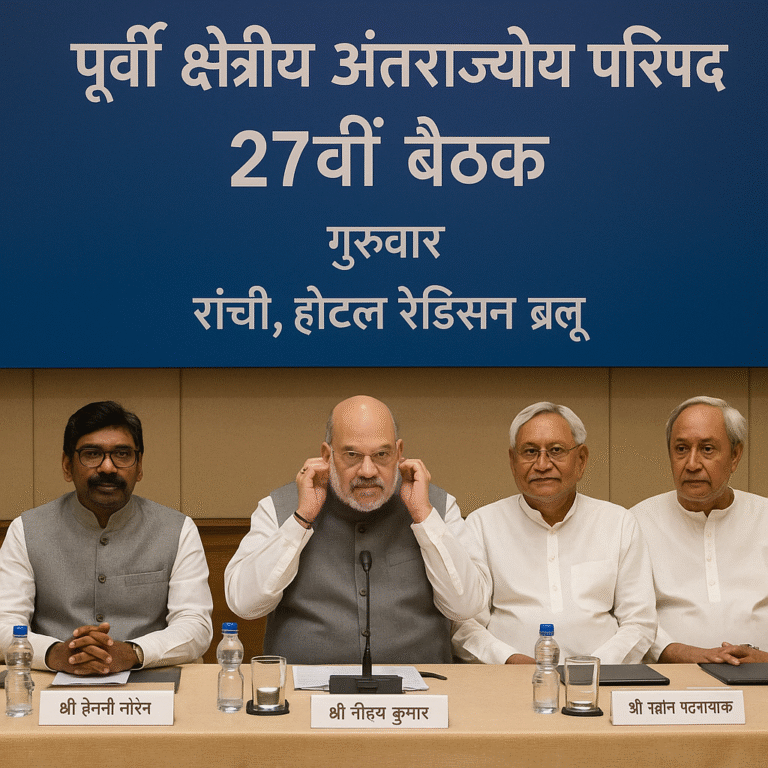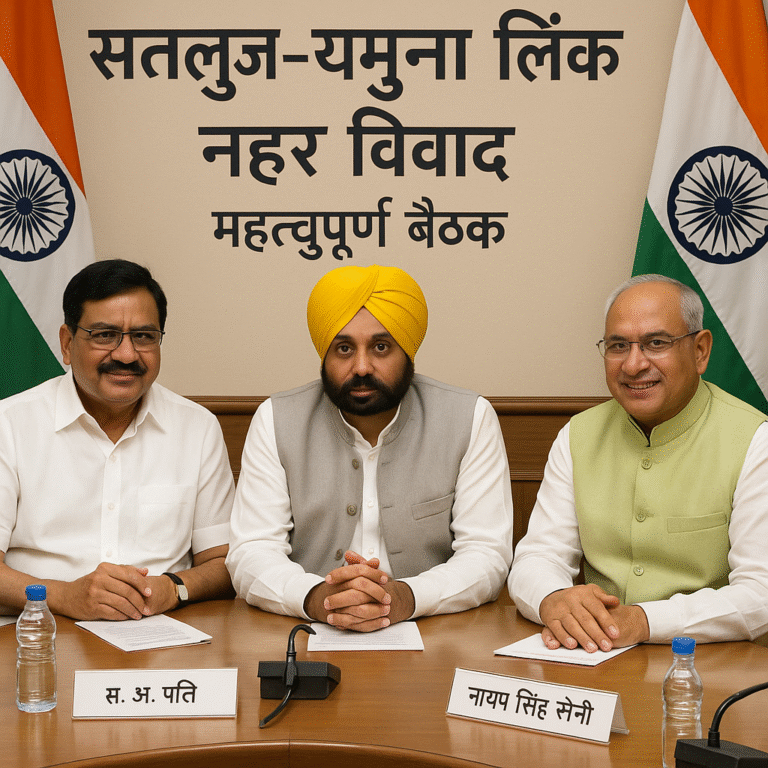संवाददाता: | 10.07.2025 | Mission Sindoor |
भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने बुधवार को नई दिल्ली में “नमामि गंगे” कार्यक्रम के अंतर्गत स्मार्ट रिवर मैनेजमेंट को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य नदियों के पुनर्जीवन के लिए नवाचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाना था। इस दौरान IIT-BHU, IIT-दिल्ली, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) और नीदरलैंड सरकार के प्रतिनिधियों ने अपने इनोवेटिव प्रस्ताव प्रस्तुत किए।
बैठक के दौरान मंत्री पाटिल ने तकनीकी नवाचार, अनुसंधान की वैज्ञानिक गहराई और सामूहिक दृष्टिकोण की सराहना की, जिसे विभिन्न भागीदारों द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने विशेष रूप से IIT BHU और IIT दिल्ली की टीमों द्वारा विकसित किए गए मॉडल्स और योजनाओं की प्रशंसा की। मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये नवाचार और अनुसंधान केवल कागज़ों तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें जमीन पर वास्तविक कार्यों में परिवर्तित किया जाए।
इस बैठक की सबसे प्रमुख पहल IIT दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किया गया वह रोडमैप था जिसके तहत IND-RIVERS पहल के अंतर्गत एक “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना की जाएगी। यह केंद्र न केवल व्यावहारिक अनुसंधान को गति देगा, बल्कि जल प्रबंधन क्षेत्र में स्टार्टअप्स को प्रशिक्षण और पोषण देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में भी कार्य करेगा। यह केंद्र राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और नीदरलैंड सरकार के सहयोग से स्थापित किया जाएगा।
मंत्री पाटिल ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता “अविरल और निर्मल गंगा” की संकल्पना को लेकर अडिग है। उन्होंने सभी हितधारकों को निर्देश दिए कि वे नवाचार आधारित पहलों को तेजी से लागू करें और इन्हें देश के अन्य प्रमुख नदी तंत्रों में भी दोहराएं। साथ ही, उन्होंने कहा कि स्मार्ट रिवर मैनेजमेंट की यह प्रक्रिया केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी पर भी आधारित होनी चाहिए।
आईआईटी दिल्ली में भारत-नीदरलैंड साझेदारी से जल प्रबंधन का भविष्य आकार लेता हुआ
देश की प्रमुख तकनीकी संस्था आईआईटी दिल्ली में एक क्रांतिकारी परियोजना की शुरुआत हुई है, जो भारत के जल संसाधन प्रबंधन को 21वीं सदी की जरूरतों और तकनीकी प्रगति से जोड़ने का कार्य कर रही है। यह पहल राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga – NMCG), भारत सरकार, और नीदरलैंड सरकार के संयुक्त सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना का लक्ष्य न केवल नदियों के पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य की बहाली है, बल्कि जल नीति, डेटा विज्ञान और स्टार्टअप संस्कृति के समागम से स्मार्ट रिवर मैनेजमेंट का एक नया वैश्विक मॉडल खड़ा करना है।
परियोजना के प्रमुख उद्देश्य (Detailed Objectives):
स्मार्ट रिवर मैनेजमेंट हेतु गहन और अंतर्विषयी अनुसंधान
परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है—अनुसंधान। जल विज्ञान, पर्यावरण इंजीनियरिंग, रिमोट सेंसिंग, GIS, जल गुणवत्ता विश्लेषण, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं द्वारा अत्याधुनिक अनुसंधान किए जा रहे हैं।
इन प्रयासों का लक्ष्य है कि देश की प्रमुख नदियाँ—गंगा, यमुना, गोमती और अन्य सहायक नदियाँ—जो जन-जीवन, कृषि और जैव विविधता की रीढ़ हैं, उनके लिए दीर्घकालिक, वैज्ञानिक और टिकाऊ प्रबंधन रणनीतियाँ विकसित की जाएं।
इसके अंतर्गत जल प्रवाह, प्रदूषण भार, बायोडायवर्सिटी इंडेक्स, नदी तटीय भूमि उपयोग परिवर्तन आदि पर डेटा संग्रह और विश्लेषण का कार्य भी शामिल है।
जल-आधारित स्टार्टअप्स को प्रशिक्षण और पोषण
परियोजना का दूसरा पहलू नवाचार और उद्यमिता को समर्पित है। भारत में जल क्षेत्र में नवाचार कर रहे युवा स्टार्टअप्स को:
वैज्ञानिक व तकनीकी मार्गदर्शन
वित्तीय सहायता व अनुदान
इनक्यूबेशन सपोर्ट (प्रारंभिक संचालन सहयोग)
सरकारी नीति व नियामक परामर्श
इंडस्ट्री कनेक्ट और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्किंग के अवसर
प्रदान किए जा रहे हैं।
इससे भारत में जल क्षेत्र आधारित स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और जल संकट जैसे वैश्विक मुद्दों पर भारतीय नवाचार वैश्विक मंचों पर पहचान बना सकेंगे।
डेटा-आधारित निगरानी प्रणाली का विकास (Smart River Monitoring Systems): नदियों के संरक्षण में तकनीक की क्रांति
जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिक विकास के दबावों के बीच, भारत की नदियाँ आज गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं। इन परिस्थितियों में परंपरागत निगरानी प्रणालियाँ, जो अक्सर सीमित आंकड़ों, मैनुअल निरीक्षण और देरीपूर्ण विश्लेषण पर आधारित होती थीं, अब अप्रासंगिक होती जा रही हैं। इस चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में, आईआईटी दिल्ली में आरंभ की गई परियोजना “स्मार्ट रिवर मैनेजमेंट” के अंतर्गत विकसित की जा रही डेटा-आधारित निगरानी प्रणाली (Smart River Monitoring Systems) एक युगांतकारी पहल के रूप में उभर रही है।
यह प्रणाली न केवल नदियों की रीयल-टाइम स्थिति पर नजर रखने की क्षमता रखती है, बल्कि यह पूर्व चेतावनी, नीति निर्णयों के लिए सटीक आंकड़े, और स्थायी जल प्रबंधन में भी क्रांतिकारी भूमिका निभा रही है।
मुख्य तकनीकी अवयव (Core Technological Components):
सैटेलाइट इमेजरी (Satellite Imagery):
उपग्रह चित्रों का प्रयोग नदियों और उनके तटीय क्षेत्रों में हो रहे भौगोलिक और पर्यावरणीय परिवर्तनों को समझने के लिए किया जा रहा है। इससे निम्नलिखित में सहायता मिल रही है:
तटीय भूमि उपयोग में बदलाव (जैसे शहरीकरण, कृषि विस्तार) की निगरानी
बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान और मॉडलिंग
औद्योगिक या घरेलू प्रदूषण के स्रोतों का स्थान निर्धारण
जल निकायों के सिकुड़ने या फैलने की प्रवृत्ति की दीर्घकालिक समझ
इन आंकड़ों को विश्लेषण कर नीति-निर्माताओं को अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियाँ तैयार करने में मदद मिल रही है।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) डिवाइसेज़:
नदी के जल में बदलाव लगातार हो रहे होते हैं। इन बदलावों की निगरानी के लिए सेंसर-आधारित IoT डिवाइसों को नदी किनारे और जलधाराओं में स्थापित किया जा रहा है, जो हर कुछ मिनटों में डेटा रिकॉर्ड कर भेजते हैं:
जल गुणवत्ता संकेतक: पीएच, घुलित ऑक्सीजन (DO), जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD), विद्युत चालकता आदि
जल प्रवाह और तापमान
घरेलू या औद्योगिक प्रदूषकों की उपस्थिति
रीयल-टाइम डेटा से यह तुरंत पता चल जाता है कि कोई प्रदूषण फैलाने वाली घटना हुई है या कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स (AI & Big Data):
IoT और सैटेलाइट से आने वाले विशाल डेटा को AI एल्गोरिद्म और मशीन लर्निंग तकनीकों की मदद से प्रोसेस किया जा रहा है, जिससे:
जटिल रुझानों और व्यवहार पैटर्न की पहचान होती है (जैसे प्रदूषण में मौसमी वृद्धि)
पूर्वानुमान मॉडल बनाए जा सकते हैं जो बाढ़, सूखे या प्रदूषण की घटनाओं की चेतावनी पहले से दे सकें
प्रभाव मूल्यांकन (impact assessment) हो सकता है—जैसे किसी फैक्ट्री द्वारा नदी पर प्रभाव
इससे सरकार और एजेंसियाँ समय रहते कदम उठा सकती हैं और ज़मीनी कार्यों को वैज्ञानिक निर्देशों से जोड़ सकती हैं।
डैशबोर्ड आधारित रिपोर्टिंग (Interactive Dashboards):
जमीन पर सक्रिय अधिकारियों, नीति-निर्माताओं और आम नागरिकों के लिए एक यूज़र-फ्रेंडली डैशबोर्ड इंटरफेस विकसित किया गया है, जो निम्नलिखित कार्य करता है:
रीयल-टाइम डेटा विज़ुअलाइज़ेशन (चार्ट्स, मैप्स, अलर्ट्स)
नदी की वर्तमान सेहत स्कोर (Water Health Index)
माहवारी या मौसमी तुलना
पॉलिसी अलर्ट्स और रिपोर्ट जेनरेशन
इससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसी भी समस्या की जन-जागरूकता और भागीदारीपूर्ण समाधान को बढ़ावा मिलता है।
संभावित लाभ (Anticipated Benefits):
प्रदूषण की त्वरित पहचान और नियंत्रण:
रीयल-टाइम निगरानी से तत्काल प्रदूषणकारी गतिविधियाँ चिन्हित कर उचित कार्रवाई की जा सकती है।
आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System):
बाढ़ या सूखे जैसे प्राकृतिक संकटों की भविष्यवाणी कर जीवन और संपत्ति की रक्षा संभव हो सकेगी।
जल गुणवत्ता में सुधार:
निरंतर ट्रैकिंग और हस्तक्षेप से जल स्रोतों को साफ और स्वस्थ बनाए रखना सरल होगा।
नीति निर्माण में पारदर्शिता और वैज्ञानिकता:
निर्णय अब अनुमानों के आधार पर नहीं, बल्कि डेटा-प्रेरित साक्ष्यों पर आधारित होंगे।
नागरिकों की सहभागिता और भरोसा:
ओपन डेटा और विज़ुअल डैशबोर्ड से जनता नदियों की स्थिति को समझ पाएगी और सक्रिय भागीदार बन सकेगी।
नीति निर्माण के लिए वैज्ञानिक सलाह और साक्ष्य-आधारित निर्णय समर्थन
भारत में जल नीति लंबे समय तक अनुमान और पूर्व अनुभवों पर आधारित रही है। यह परियोजना डेटा-संचालित और वैज्ञानिक परामर्श पर आधारित नीति निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत:
सरकारों को वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर परामर्श
जल संसाधन प्रबंधन अधिनियमों में सुधार हेतु सुझाव
अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का स्थानीयकरण
राज्यों और नगर निकायों के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देश
उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे नीति निर्माण अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और प्रमाणिक हो सके।
प्रभाव क्षेत्र (Geographical Scope and Reach):
इस परियोजना का भौगोलिक प्रभाव सीमित नहीं है। यह केवल गंगा पर केंद्रित न होकर, यमुना, गोमती, काली, सोन, रामगंगा जैसी प्रमुख नदियों के साथ-साथ पूरे गंगा बेसिन क्षेत्र को कवर करता है, जो देश के 11 राज्यों और 40% आबादी को प्रभावित करता है। परियोजना की सफलता के बाद इसे अन्य नदी प्रणालियों जैसे नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र पर भी लागू करने की योजना है।
संभावित दीर्घकालिक प्रभाव (Long-Term Impact):
वैश्विक जल प्रबंधन मानकों की स्थापना: भारत इस परियोजना के माध्यम से जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी बनने की दिशा में अग्रसर है।
विकासशील देशों के लिए मॉडल: अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण अमेरिका के देश इस मॉडल को स्थानीय रूप से अपना सकते हैं।
जलवायु अनुकूलता में वृद्धि: डेटा-आधारित स्मार्ट प्रबंधन से बाढ़, सूखा और जल संकट की मार को कम किया जा सकेगा।
सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण: जल गुणवत्ता में सुधार, नदी किनारे की आजीविका, पर्यटन और स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा।
नवाचार आधारित हरित अर्थव्यवस्था: जल क्षेत्र में स्टार्टअप्स और तकनीकी समाधान भारत में एक हरित और सतत आर्थिक मॉडल को जन्म देंगे।